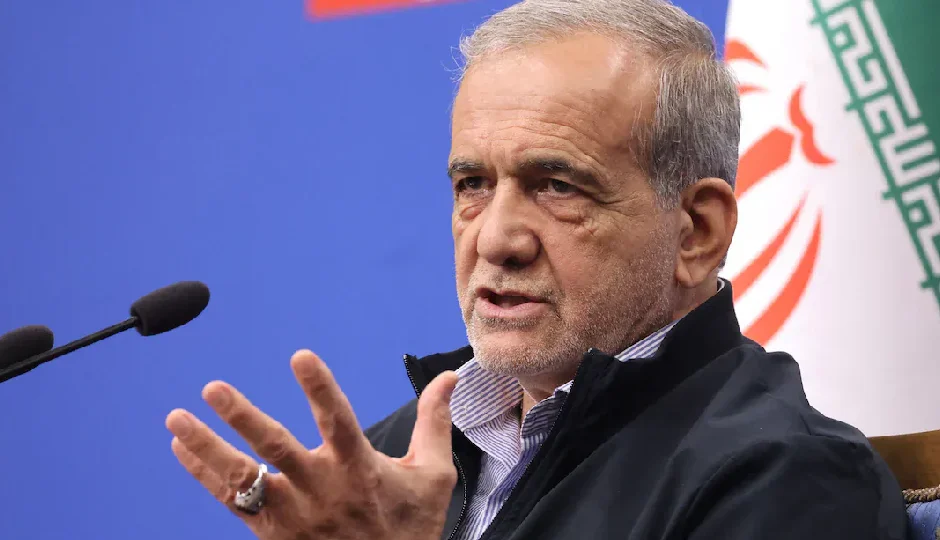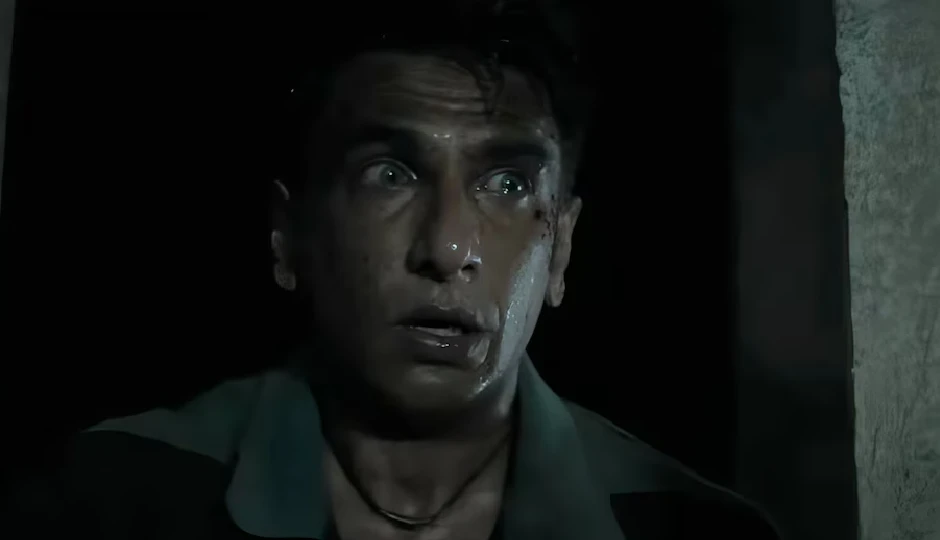सनातन दर्शन में मानव जीवन को केवल सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा माना गया है। इस यात्रा के चार पड़ाव बताए गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ और काम जीवन की व्यवस्था को संतुलित रखते हैं, जबकि मोक्ष इस समस्त यात्रा का परम लक्ष्य है। लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि मोक्ष वास्तव में है क्या? क्या यह सबके लिए आवश्यक है या केवल संन्यासियों का विषय है? वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने मोक्ष के अर्थ को सरल शब्दों में समझाते हुए इसके वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। आइए जानते हैं उनके विचारों के माध्यम से मोक्ष की सच्ची परिभाषा।
आत्मा कभी बंधन में नहीं होती
प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि मनुष्य स्वयं को बंधा हुआ मानता है, जबकि वास्तव में आत्मा कभी किसी बंधन में पड़ती ही नहीं। त्रिगुणों से बने शरीर और अहंकार की बुद्धि के कारण हमें यह भ्रम होता है कि हम बंधन में हैं। वे गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई का उल्लेख करते हैं—
“जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटति कठिनई।” अर्थात अज्ञानवश जड़ और चेतन के बीच एक गांठ पड़ गई है। यह गांठ झूठी है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से मुक्त है, फिर भी इसे खोलना कठिन प्रतीत होता है। यही अज्ञान मनुष्य को बार-बार जन्म-मरण के चक्र में बांधे रखता है।
भ्रम के समाप्त होते ही मोक्ष का अनुभव
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि शुद्ध “मैं” ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन वही अपने असली रूप को भूलकर शरीर से स्वयं को जोड़ लेता है। मनुष्य तीन शरीरों से बना होता है—स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जब हमसे पूछा जाता है कि “आप कौन हैं?”, तो उत्तर अक्सर शरीर और पहचान तक सीमित रहता है—नाम, जाति, स्थान। जबकि यह सब केवल स्थूल शरीर से जुड़ी पहचान है। जब यह भ्रम टूट जाता है कि “मैं यही शरीर हूं”, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। भ्रम का नाश ही वास्तव में मुक्ति है।
आत्मा है साक्षी, निरपेक्ष और स्वतंत्र
प्रेमानंद महाराज समझाते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव होता है, उसे हम अपना अनुभव मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को देखने पर हम कहते हैं—“मैंने देखा।” जबकि वास्तव में देखने का कार्य नेत्र इंद्रिय करती है, मन उस अनुभव को ग्रहण करता है और आत्मा केवल साक्षी बनी रहती है। आत्मा न तो देखने वाली है, न सुनने वाली और न करने वाली—वह केवल प्रकाश स्वरूप है, जिससे मन और इंद्रियों को शक्ति मिलती है। इसी कारण आत्मा निरपेक्ष है, किसी क्रिया से बंधी हुई नहीं।
अहंकार ही वास्तविक बंधन है
भगवद्गीता के पांचवें अध्याय का उल्लेख करते हुए प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है। वह देखता हुआ भी नहीं देखता, खाता हुआ भी नहीं खाता। इसका अर्थ यह है कि क्रियाएं इंद्रियां करती हैं, मन संकल्प करता है, लेकिन आत्मा केवल साक्षी रहती है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि “मैंने किया, मैंने देखा”, तभी अहंकार जन्म लेता है और वहीं से बंधन शुरू होता है। अहंकार के मिटते ही मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाता है।
गुरु कृपा से खुलता है मुक्ति का मार्ग
प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि इस सत्य का अनुभव केवल पुस्तकों से नहीं होता। तुलसीदास जी की पंक्ति “छूटति कठिनई” इसी ओर संकेत करती है कि बिना गुरु कृपा और साधना के यह भ्रम आसानी से नहीं टूटता। गुरु की कृपा से जब साधना मिलती है, तब धीरे-धीरे यह अनुभूति होती है कि “मैं शरीर नहीं हूं।” शरीर केवल वस्त्र के समान है—जैसे कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति कुर्ता नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति को चोट लगने पर पीड़ा तो होती है, लेकिन दुख नहीं होता। यही अवस्था जीवनमुक्त महापुरुष की होती है, जो संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त होता है।